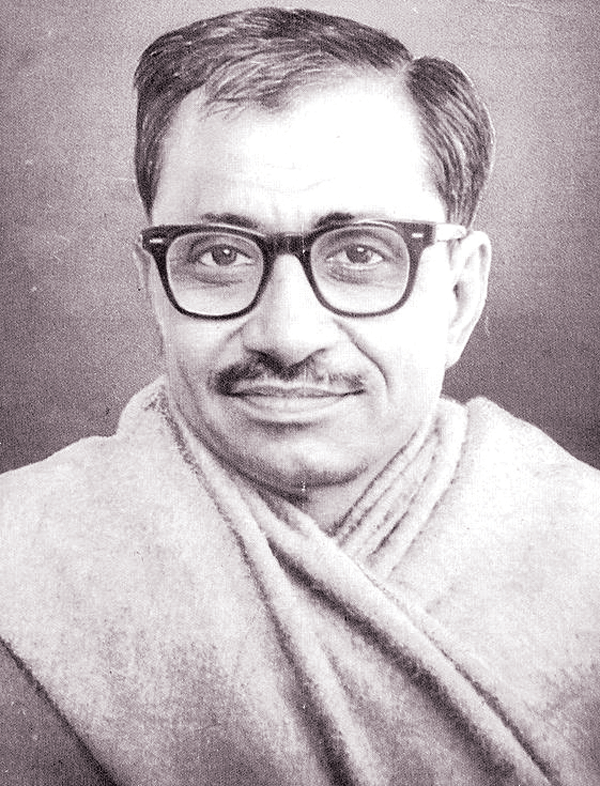दीनदयाल उपाध्याय
शिक्षा का संबंध जितना व्यक्ति से है, उससे अधिक समाज से। हम ऐसे मानव की कल्पना कर सकते हैं, जिसे किसी भी प्रकार की शिक्षा न मिली हो और जो अपनी सहज प्रवृत्तियों के सहारे ही जीवन-यापन करता हो, किंतु बिना शिक्षा के समाज संभव नहीं। किसी काल विशेष में कोई मानव समूह मात्र समाज की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। उस समूह में प्रत्येक क्षण कुछ व्यक्ति घटते और कुछ बढ़ते रहते हैं। मानव की आयु मर्यादा के अनुसार एक कालावधि में किसी भी मानव समूह के सभी घटक भौतिक दृष्टि से बदल जाते हैं। किंतु इसके उपरांत भी यदि उस मानव समूह का व्यक्तित्व एवं उसकी चेतना बनी रहे, नए घटकों को पुराने घटकों से अपने संबंध का भान रहे तथा वे पुराने घटकों की जीवन की अनुभूति को अपनी अनुभूति मानकर और समझकर आगे चलें, तो उस समूह को ‘समाज’ नाम प्राप्त हो जाता है। अर्थात् एक के बाद एक मानव जब दूसरों को जो प्रायः उसके बाद जनमे हों, विभिन्न क्षेत्रों के अपने संपूर्ण अनुभव को अथवा उसमें के सारभूत अंश को विभिन्न उपायों द्वारा प्रदान या संसर्गित करता है, तो इस प्रक्रिया में एक निरंतर गतिमान मानव समूह की सृष्टि होती है, जिसे समाज कहते हैं। अनुभव प्रसारण की इस क्रिया को ही वास्तव में ‘शिक्षा’ कहते हैं। यदि शिक्षा न हो तो ‘समाज’ का जन्म ही न हो। अतः शिक्षा के प्रश्न को मूलतः सामाजिक दृष्टिकोण से ही देखना होगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार यह ऋषि ऋण है, जिसे चुकाना प्रत्येक का कर्तव्य है। जब हम भावी संतति की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, वास्तव में हमारी उनके प्रति उपकार की भावना नहीं रहती, अपितु हमें जो कुछ धरोहर अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, उसे आगे की पीढ़ी को सौंपकर उनके ऋण से उद्धरण होने की मनीषा रहती है। जॉन बुकन ने इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है, हम भूत के ऋण से उऋण हो सकते हैं, यदि हम भविष्य को अपना ऋणी बनाएं।
शिक्षा संस्थाएं
‘शिक्षा’ की जितनी व्यापक और गहरी व्यवस्था होगी, समाज उतना ही अधिक पुष्ट और गंभीर होगा। नई पीढ़ी के जितने लोगों को और जितनी अधिक मात्रा में पिछली ज्ञान निधि प्राप्त होगी, उसी पंूजी को लेकर वह जीवन के कार्यक्षेत्र में उतरेगी। यह भी स्वाभाविक है कि वह प्राप्त पूंजी में अपने प्रयत्न और अनुभव के आधार पर वृद्धि करे। इस प्रकार यह पूंजी बराबर बढ़ती जाएगी। किंतु इसके लिए जहां शिक्षा की व्यापक और विविधतापूर्ण योजना करनी होगी, वहां ‘प्रदेय’ के असारभूत अंगों का परित्याग एवं तत्त्व का संरक्षण भी बड़े मनोयोग से करना होगा। एतदर्थ ऐसे लोगों की आवश्यकता हो जाती है, जो पीढ़ियों के संचित ज्ञान को आत्मसात् करके सुबोध बना सकें। ‘शिक्षा’ के व्यापक अर्थों में समाज का प्रत्येक घटक ‘शिक्षक’ होने के उपरांत भी उपर्युक्त कारणों से ‘शिक्षण संस्था’ का उदय हुआ।
राष्ट्र जीवन के ‘मानस’ का ज्ञान
प्रत्येक पीढ़ी के साथ समाज की प्राचीन निधि का संरक्षण, संवर्धन एवं आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरण होता रहता है। किंतु नई अनुभूतियों का जब तक प्राचीन अनुभूतियों के साथ एकीकरण नहीं होता, तब तक वे ‘समाज’ के मानस में स्थान नहीं पा सकतीं। यह तभी संभव है, जबकि समाज’ के आज तक के संपूर्ण अनुभवों और जीवन व्यापारों का समन्वित, एकीकृत, सुसंबद्ध एवं सर्वांश में व्यापक ज्ञान प्राप्त हो। इस ज्ञान की छाप जितनी गहरी, सुस्पष्ट और सुव्यवस्थित रहेगी, उतना ही मानव अपनी जीवन यात्रा में सरलता और शांति से पग बढ़ा सकेगा। यदि उसको अपने राष्ट्र के ‘मानस’ का ठीकठीक ज्ञान नहीं हो तो वह अपने जीवन में सदैव ही उखड़ा-उखड़ा सा अनुभव करेगा।
शिक्षा के माध्यम
राष्ट्र मानस के ज्ञान अथवा शिक्षा के प्रमुख माध्यम हैं-1. संस्कार, 2. अध्यापन और 3. स्वाध्याय। मनुष्य अनजाने ही अपने चारों ओर के समाज से संस्कार ग्रहण करता रहता है। उसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक’ का काम करता है। ‘संस्कार’ यद्यपि दोनों ओर से चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि मानस की अनुकरण (Imitation), संवेदना (Sympathy) एवं सूचनात्मक (Suggestion) प्रवृत्तियों के नियम के अनुसार समर्थ कर्ता की क्रियाएं ही प्रभावकारी होती हैं। स्वभावतः पिछली पीढ़ी के आचार-विचारों का संस्कार नई पीढ़ी पर पड़ता है। माता-पिता, परिजन, पुरजन, गुरुजन, अग्रपाठी, सहपाठी, समाज के नेता और अधिष्ठाता ये सभी विभिन्न प्रकार से निरंतर संस्कार डालते रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी क्रियाओं का परिणाम केवल उन पर ही नहीं, बल्कि अन्यों पर भी पड़ता है। स्वयं को ही नहीं, अन्यों को भी वे अपने कर्म बंधन में बांधते हैं।
अध्यापन व लोकशिक्षा
‘अध्यापन’ शिक्षा का सर्वसामान्य साधन है। साधारणतया’ अक्षर ज्ञान’ तथा पाठ्यपुस्तकों अथवा तत्संबंधी पाठ्यक्रम का अध्यापन ही इस क्षेत्र के अंतर्गत समझा जाता है। किंतु वास्तव में यह क्षेत्र भी बहुत विस्तीर्ण है। मानव के ज्ञान का बहुत ही थोड़ा अंश भाषा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और उसमें से भी एक अंश मात्र लिपिबद्ध है। अत: लिपि ज्ञान अथवा भाषा ज्ञान से शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।’ अध्यापन के अंतर्गत वे सब क्रियाएं आती हैं, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपने पास के ज्ञान को दूसरे को देने का चेतनापूर्वक प्रयास करता हो। यह प्रयास पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों में ही नहीं, घर-घर में तथा खेत-खलिहान, कारख़ानों, दुकानों, पाठशालाओं, कलाभवनों, खेल के मैदानों और मल्ल शालाओं में भी चलता रहता है। साथ ही जीवन के पहले आश्रम में ही नहीं, बाद में भी मनुष्य का विभिन्न प्रकार से अध्यापन होता रहता है। प्राचीन काल से कथा और कीर्तन तथा आज के रेडियो, सिनेमा, समाचार-पत्र आदि सभी इस सीमा में आते हैं।
स्वाध्याय
‘स्वाध्याय’ मनुष्य का स्वयं का अध्यापन है। लिपि ज्ञान स्वाध्याय के लिए बहुत आवश्यक है। पठन, मनन और चिंतन के सहारे मनुष्य ज्ञान को आत्मगम्य करता है। बिना स्वाध्याय के न तो प्राप्त ज्ञान टिकता है और न बढ़ता है। स्वाध्याय के बिना ज्ञान को जीवन का अंग बनाकर ‘तेजस्वीय’ बनाने का तो प्रश्न ही नहीं। अतः ‘स्वाध्यायान्मा प्रमदः’-यह कुलपति का स्नातक को दीक्षांत के अवसर पर आदेश रहता था। पुस्तकालय आदि की व्यवस्था स्वाध्याय के लिए आवश्यक है।
शिक्षा का यदि सर्वांगपूर्ण विचार किया जाए तो शालेय शिक्षा क्रम तथा उसका माध्यम क्या हो, यह सहज ही समझा जा सकता है। व्यक्ति यदि भूत की ज्ञान निधि को भविष्य तक पहुंचाने वाला एक अभिकर्ता मात्र है, तो उसकी शिक्षा में इसका समावेश होना चाहिए। यदि यह नहीं हुआ तो वह समाज का चेतनशील एवं प्रभावी घटक होने के स्थान पर समाज से असंबद्ध एवं मृत प्राण जैसा होकर समाज के लिए अहितकर ही होगा।
शालेय शिक्षा अकेली ही मनुष्य का निर्माण नहीं करती। संस्कार और अध्यापन का बहुत सा क्षेत्र ऐसा है, जो शालेय क्षेत्र से बाहर है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में विरोध रहा तो विद्यार्थी के जीवन में एक अंतर्द्वद्व उपस्थित हो जाता है। एक समन्वित, एकीकृत, सर्वांगपूर्ण, अखंड व्यक्तित्व का विकास होने के स्थान पर उसकी प्रकृति में विभक्त निष्ठाओं का समावेश हो जाता है। समाज और उसके बीच एक खाई पड़ जाती है। इस दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि शिक्षा का माध्यम स्वभाषा ही हो सकती है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, वह स्वयं भी एक अभिव्यक्ति है। भाषा के एक-एक शब्द, वाक्य-रचना, मुहावरों आदि के पीछे समाज के जीवन की अनुभूतियां, राष्ट्र की घटनाओं का इतिहास छिपा हुआ है। फिर स्वभाषा व्यक्ति को अलग-अलग प्रकोष्ठों में नहीं बांटती।
शिक्षा के इस सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया तो व्यक्ति सहज ही चतुर्विध पुरुषार्थों के लिए प्रयत्न की योग्यता और सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा।
-पांचजन्य, नवंबर 10, 1958