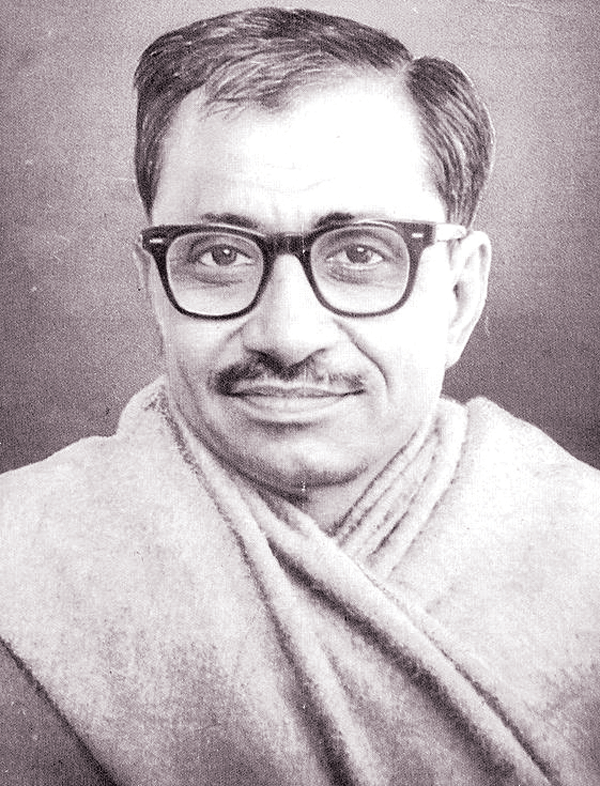दीनदयाल उपाध्याय
समाज की उन्नति का अर्थ क्या है? वैभव का चित्र कौन सा हो, यह कल्पना से रंगा जा सकता है। यदि हमने बुद्धि लगाई तो वैज्ञानिक ढंग से तारतम्य भी बैठाया जा सकता है। कारण मीमांसा भी दी जा सकती है। वास्तविकता यह है कि जीवमान समाज का चित्र कुछ चौखटों में बांधा नहीं जा सकता। सौ वर्ष बाद क्या करेंगे, समाज का क्या चित्र होगा? इसका उत्तर भी वैसा ही है, जैसे बीरबल ने पृथ्वी के केंद्र के संबंध में बताया, पहले तो उन्होंने कहा कि छह महीने की मोहलत और पैसा चाहिए। साथ ही कुछ रस्से और खूंटियां मंगवाकर रख लीं। जंगल में तालाब के बीच में एक खूंटा भी गाड़ दिया और कहा कि यह है पृथ्वी का केंद्र। इसी तरह चौसर खेलने के लिए बैठिए। पचास दांव के हिसाब से गोटी कहां होगी, कहना कठिन है। प्रवृत्तियों का विचार किया जा सकता है। कारण मीमांसा भी दी जा सकती है। किंतु कौन-कौन अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कौन उठेंगे, कहना कठिन है। आज से पचास वर्ष बाद मजदूर, किसान, मिल-मालिक, दुकानदार का क्या संबंध होगा, क्या बनेगा-यह भी कहना कठिन है। भविष्य के बारे में जीवमान समाज का क्या बनेगा, यह भी कहना कठिन है। निर्जीव के लिए तो गति के नियम से हिसाब लगाकर कुछ कहा जा सकता है। ईंट, पत्थर तो चुनकर मकान बनेगा ही। मानव की प्रकृति, प्रवृत्तियां अध्ययन कर बताया जा सकता है। परिणाम सोचे जा सकते हैं। Minutest details नहीं बनाई जा सकतीं।
संगठन और उसके द्वारा वैभव का हमने विचार किया। वैभव की सर्वसाधारण कल्पना छोटी-मोटी रूपरेखा में नहीं हो सकती। हमने अपनी प्रार्थना में उसे व्यक्त भी किया है। परमात्मा से शुभ आशीर्वाद मांगा है। सीधा आशीर्वाद नहीं मांगा। कुछ बातें उसके साथ जोड़ दीं। इस बारे में एक कथा याद आ गई। एक व्यक्ति अंधा होने के साथ-साथ निर्धन और निसंतान भी था। उसने शिवजी की आराधना की। प्रसन्न होकर प्रभु ने उससे कहा कि एक वरदान मांगो। उसे एक ही वरदान मांगना था। इसलिए उसने सोच-विचार किया कि यदि आंखें ही मांगी तो वह निःसंतान और निर्धन ही रह जाएगा और यदि वह संतान मांग लेता है तो भी वह अंधा और गरीब ही रहेगा, इसलिए उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने पोते को सोने के बरतन में खीर खाते हुए देखूं तो इस तरह उसने समझदारी से सभी कुछ एक ही वरदान में मांग लिया। इसी तरह हमने भी तीन वरदान मांगे कि प्रभु तुम्हारे आशीर्वाद से यह कार्यशक्ति वैभव पर पहुंचाने में समर्थ हों। हमने ताकत से मांगा, कृपा से नहीं। केवल कृपा से जो मिले, वह छिन भी जाता है। भस्मासुर ने भगवान् के सिर पर हाथ रखकर उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन वह उलटा ही हुआ। ‘विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम्’ इसमें अपने वैभव की कल्पना और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों स्पष्ट कर दिए।
जहां पर धर्म नहीं है, वहां पर हमने वैभव ही नहीं माना। धर्म का संरक्षण और वैभव की प्राप्ति दो क्रियाएं हैं। मान लो, बाजार जाकर पुस्तक खरीदनी है। ये दो क्रियाएं हैं। बाजार पहुंचकर पुस्तक खरीदें, यह भी संभव है। यदि क़िताब न मिले या कोई दूसरी खरीद लाएं तो भी ये दो भिन्न-भिन्न क्रियाएं होंगी, लेकिन पानी पीकर प्यास बुझाना, दो भिन्न क्रियाएं नहीं हैं! क्योंकि प्यास तो पानी पीकर ही बुझेगी। बिना पानी पिए प्यास बुझेगी ही नहीं। इसी तरह धर्म का संरक्षण और राष्ट्र का वैभव दोनों एक साथ हो सकते हैं। धर्म के संरक्षण से ही राष्ट्र का वैभव हो सकता है। ये दोनों बातें अलग नहीं हो सकतीं। धर्म का संरक्षण, राष्ट्र का वैभव और संगठित कार्यशक्ति, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। चोरों में भी अनुशासन, संगठन, त्याग होता है। तस्कर, नाजायज शराब बनाने वालों, जुआ खेलने वालों के भी संगठन होते हैं, लेकिन हमारा संगठन धर्म के आधार पर होता है। समाज और व्यक्ति दोनों का विकास करना चाहिए।
धर्म ही उसका आधार है। इसकी पहली व्याख्या है कि धर्म से ही धारणा हो सकती है। धर्म की अलग-अलग परिभाषाएं हो गई हैं। इसलिए सोचना पड़ेगा कि धर्म क्या है, क्योंकि कोई संस्कृति को लेकर धर्म की बातें करता है और कोई जाति-पाति पर विश्वास करने को धर्म समझने लगता है। हरिजनों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। हरिजनों ने कहा कि भगवान् और भक्त के बीच में कौन बाधक बनते हैं? क्यों बनते हैं? उन लोगों ने धर्म का अर्थ छुआछूत, भेदभाव को समझ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म को छोड़ना ही अच्छा है। एक बार एक अपराधी मामलों के वकील के पास एक सज्जन आए। उन्होंने बताया कि हमने बहुत से बुरे काम किए-डाके डाले, लड़कियां उठाईं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उनसे पूछा गया कि धर्म कैसे नहीं छोड़ा। तो उन्होंने बताया कि किसी के हाथ का बना भोजन नहीं किया, बिना चौका लगाए नहीं किया। तो धर्म का अर्थ क्या है? यह प्रश्न कठिन है। महाभारत काल में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा कौन सा रास्ता है, जिस पर सब चलें। युधिष्ठिर का उत्तर था, ‘धर्म का रास्ता।’ लेकिन इसका अर्थ छिपा हुआ है। धर्म के बारे में मतभेद है। कुछ लोगों ने धर्म का अर्थ पूजा-पाठ आदि को ही कहा। मुसलमानों की ओर देखो, उनका एक पैगंबर, एक किताब और एक पद्धति होती है। ईसाई और यहूदी भी ऐसे ही होते हैं। यहां कोई एक किताब नहीं है। वेदों को कोई मानता है, कोई नहीं मानता।
अस्सी प्रतिशत दुनिया तो प्राय: अज्ञानवश ऐसा सोचती है कि यह तो मेरा धर्म नहीं है। आकाश पर सितारे इधर-उधर बिखरे हुए अव्यवस्थित से दीखते हैं। ज्योतिषी तो इन सबकी व्यवस्था को समझता है, किंतु हम नहीं समझ सकते। यह पद्धति है कि हम सबके अनुसार धर्म का अर्थ नहीं लगाते। हमारे यहां विचारों की स्वतंत्रता है, किंतु मुसलमानों में कुरान की बात को ही मानकर चलते हैं। उसके बारे में लिखा है, ‘अकल को दखल नहीं’। वहां विचारों में स्वतंत्रता होते हुए भी भेद है। जैसे शिया, सुन्नी इत्यादि। ईसाइयों में कितने चर्च होते हैं। केवल दूर से ही एकता दिखाई देती है। जैसे पहाड़ की एकरूपता दूर से ही नज़र आती है। पास जाकर देखने पर उसमें गहरे खड्ड और खाई नजर आती हैं। हमारा इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। बाकी सभी धर्म तो हमारी तुलना में अभी दुधमुंह बच्चे हैं। सोलह मन्वंतर युग बीत गए। एकरूपता पूरी कैसे नज़र आएगी? यह आश्चर्य की बात है कि इतनी विविधता होते हुए भी हमारे में इतनी एकरूपता है और यही खुशी मनाने का कारण भी है।
एक बार एक गांव का आदमी जो प्याज और गुड़ से ही रोटी खाता था, राजा के यहां से खाने का बुलावा आने पर वहां गया। वहां भोजन देखकर रोने लगा कि यहां तो गुड़ और प्याज है ही नहीं, मैं किससे खाऊं। अत: जहां विकास होता है, वहां विभिन्नता तो होती ही है। प्रथम चरण में अमीबा होता है, उसमें एक ही कोशिका होती है, क्योंकि उसका शरीर गोल-मटोल है। मनुष्य के समान उसके अंगों का विकास नहीं हुआ है। इसलिए उसमें सौंदर्य भी नहीं है। मनुष्य को भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सभी कुछ दी हैं। उसके शरीर में अंगों का विकास हुआ है। अत: उसमें सुंदरता है। यदि उसके भी कान, नाक नहीं होते और वह भी निराकार और बुद्धिहीन होता, उसका विकास न हुआ होता तो उसमें भी सुंदरता नहीं आती।
प्रभुदत्तजी बोलते नहीं, भगवान् का ही नाम बोलते हैं, श्रीकृष्ण कहकर सबको बुलाते हैं, ‘हे नाथ’ कहकर ही सब खाना-पीना प्रारंभ करते हैं। जैसे एक-दो भावों को व्यक्त करने के लिए अनेक शब्द होते हैं, वैसे ही एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कितने ऊंचे-नीचे स्वर होते हैं। यदि कोई कहे कि अनेक स्वर निकालो, तो मूर्खता होगी। स्वरों में तालमेल चाहिए। अनेक प्रकार के स्वर एक साथ निकलेंगे तो बेसुरा लगेगा। कहीं भी ऊंचा-नीचा किया, contrasting की और सामंजस्य नहीं किया तो सब अटपटा सा लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी पागल के शब्द और उसकी तरह-तरह की आवाजें विचित्र लगती हैं। यह भी विकास नहीं कहलाता। एक-दूसरे में तालमेल और सामंजस्य चाहिए। रेखाओं में से भी सुंदर चित्र बनते हैं। जहां रेखाओं की भरमार हो, वहां साफ किया जाए। केवल विविधता ही होना अच्छा नहीं। बीच में तालमेल भी चाहिए। एक-दूसरे से संबद्ध होकर जब रेखाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं, तभी उस चित्र का विकास होता है। धर्म का काम भी इसी प्रकार है, उसमें भी एकसूत्रता चाहिए निर्माण भी करना है तो भी एकसूत्रता चाहिए। हमारे राष्ट्र की संस्कृति की विविधतामयी प्रकृति में से सामंजस्य का नाम धर्म है। जहां यह एकात्मता हो जाए वहीं धर्म है। नहीं तो विनाश ही होगा। विकृति एकसूत्रता नहीं ला सकती।
– संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : दिल्ली (9 जून, 1958)