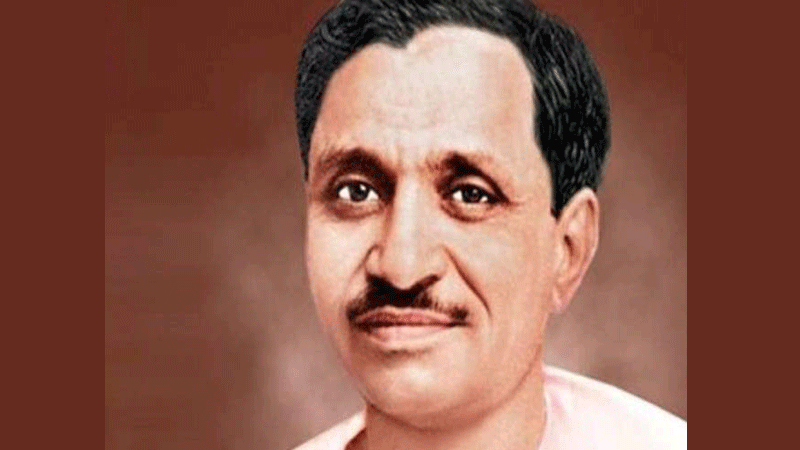दीनदयाल उपाध्याय
पिछले अंक का शेष…
मान लीजिए, आपकी जेब में चार दुअन्नियां पड़ी हैं। उसमें तीन तो अच्छी हैं और एक खोटी है। तो आप सबसे पहले किसे निकालकर देंगे। आप सोचेंगे कि यह खोटी दुअन्नी है। पहले इसे ही चला दो और जब कोई उसे नहीं लेगा तो दूसरी दुअन्नी दे देंगे। ऐसे बहत कम लोग हैं जो यह सोचते हैं कि मैं तो बेवकूफ़ बन ही गया। अब दूसरे को क्यों बनने दूं। लेकिन अधिकतर आदमी ऐसे होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं तो बेवकूफ़ बन ही गया, उसे तसल्ली तभी होती है, जब वह दूसरे को बेवकूफ़ बना देता है। इसका नतीजा यह होता है कि जब हर कोई पहले खोटे सिक्के को चलाने लगता है तो असली पैसा पीछे चला जाता है।
इस प्रकार ही धर्म के बारे में भी ऐसा ही हो गया होगा। इसकी जो असली चीज़ है, वह पीछे रह गई, बाक़ी चीजें ही आगे आती रहीं। कुछ लोग बुराइयों को देखते हुए कहते हैं कि हमें धर्म नहीं चाहिए। परंतु यह कहने से तो काम नहीं चलेगा। चलेगा भी तो कितने दिन? मान लो आपने एक बार कुछ सड़ी-गली चीज़ खा ली और उसके कारण हैजा हो गया। अब डर के मारे वह कहे कि मैं अब कभी कुछ नहीं खाऊंगा, तो वह जिंदा कैसे रहेगा? उसने फल खाया, लेकिन सड़ा हुआ। उसके भय के कारण अब वह अच्छा फल खाने से भी इनकार करता है तो यह बात ग़लत है। बिना फल खाए, बिना रोटी खाए वह जिंदा कैसे रह सकता है?
इसी तरह धर्म के बारे में है। लोगों ने धर्म का दुरुपयोग किया है। धर्म के संबंध में लोगों ने ऐसी बहुत सी चीजें चलाई होंगी, जिसके कारण लोगों के मन में आया होगा कि धर्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। धर्म के नाम पर बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े अन्याय हुए हैं। लेकिन इतना होने पर भी धर्म का जो सत्य स्वरूप है, वह सामने नहीं आया है। उसे पहचानना, सामने लाना बहुत आवश्यक है। चार लोग अगर चीज़ों में मिलावट करके बेचते हैं, हम उन चीज़ों का बेचना ही बंद करवा दें, तब तो काम नहीं चलेगा। आवश्यकता तो इसी बात की है कि लोग एडल्टरेशन न करें। मिलावट न करते हुए वे अपनी चीज़ शुद्ध रूप में कैसे बेचें, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। हम यह नहीं कर सकते कि लोगों का बेचना बंद करवा दें। सड़क पर यदि एक्सीडेंट हो गया है तो लोग सड़कों पर चलना ही बंद कर दें। यह तर्क ग़लत हैं।
यह ऐसा ही तर्क है, जैसे एक बार एक सज्जन जहाज़ से जाना चाहते थे। उनकी मां ने जहाज़ से जाने के लिए उन्हें मना कर दिया। उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता एक जहाज़ से गए थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि उसके दादा कहां मरे थे? तो बताया गया कि घर ही में मरे थे। फिर वह बोले कि मेरे चाचा को क्या हो गया था? मां ने कहा कि वे घर में ही मरे थे, बीमार थे, खाट के ऊपर ही मरे। रात को जब खाट के ऊपर सोने का वक्त आया तो उन्होंने खाट पर सोने से इनकार कर दिया। मां ने पूछा कि खाट पर क्यों नहीं सोते तो उसने जवाब दिया कि मेरे बाबा और चाचा खाट पर मर गए थे, इसलिए मैं खाट पर नहीं सोऊंगा। मां ने कहा कि बड़ा बेवकूफ़ है। ऐसा भी कोई सोचता है। तब उसने कहा कि मेरे पिता जहाज़ पर गए और मर गए तो मुझे क्यों मना करती हो? तो इस तरह यह तर्क बिल्कुल ग़लत है कि एक्सीडेंट हो गया तो सड़क पर चलना बंद कर देना चाहिए। एक्सीडेंट कैसे रोकें, इस पर विचार करना होगा।
धर्म का सत्य रूप कैसे सामने आएगा, इसका विचार करने की आवश्यकता है। जब हम धर्म का विचार करते हैं तो पहला प्रश्न सामने आता है कि धर्म का अर्थ क्या? यहां से सोचें तो धर्म का अर्थ वास्तव में एक संक्षिप्त सी व्याख्या है। यह व्याख्या यह है कि ‘धारणात धर्ममित्याह, धर्मो धारयते प्रजा’- मनुष्य को जिससे धारणा हो. वह उसका धर्म है और किसी भी चीज़ को लें। पेड़ है, पशु-पक्षी हैं, लोहा, तांबा, मिट्टी जो कुछ भी है, वही उसकी धारणा है, उसका धर्म है। सर्य से जिसकी धारणा हो, वह उसका धर्म है, यानी किसी भी चीज़ की धारणा जैसे मैंने पहले बताया कि अग्नि है तो अग्नि की धारणा उसकी दाहकता से है। अग्नि के ऊपर पानी डाल दीजिए तो क्या होगा? पानी डालने के बाद उसकी दाहकता तो समाप्त हो जाएगी। बाक़ी की अग्नि बनी रहेगी। जैसे जलते हुए कोयले पर पानी डालते हैं तो उसका स्वरूप तो वही रहता है, लेकिन दाहकता समाप्त हो जाती है और जब उसके अंदर की दाहकता निकल गई तो उसे कोई अग्नि नहीं कह सकेगा। फिर उसे बुझा हुआ कोयला कहते हैं।
इसी तरह आप देखें कि यह जो धर्म है। इसके ऊपर धारणा होनी चाहिए। यह पहली चीज़ है और जब हम पहली चीज़ को विचार करें तो हमें व्यक्ति का विचार करना होगा। धारणा होती है कि हम व्यक्ति का विचार करें, क्योंकि अपना धर्म क्या है? तो कहना होगा कि जिससे अपनी धारणा हो। जिससे हम जिंदा रह सकें। तो सामान्य चीज़ आएगी कि सब ठीक है, भोजन करना चाहिए। इससे धारणा होती है। भोजन करना धर्म है, उससे आदमी टिकता है, शरीर जिससे टिका रहे। यदि शरीर जिससे नहीं टिकता, हमने ऐसा कुछ किया तो वह अधर्म होगा। इसलिए हमारे यहां आत्महत्या करना पाप माना जाता है। यह कभी भी पुण्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें से शरीर की धारणा समाप्त होती है। तो यह धारणा रहनी चाहिए कि शरीर टिका रहे।
फिर भोजन के बारे में विचार आता है कि वही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो। यदि स्वास्थ्य ख़राब करनेवाला भोजन किया जाए, तो कहना होगा कि वह धर्म के अनुकूल नहीं है। यदि शराब पी। शराब पीने के कारण शरीर की शक्ति क्षीण होती चली जाती है तो कहना पड़ेगा कि वह धर्म नहीं है। धर्म फिर क्या है? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो सीधा सा आधार यह है कि जिसके कारण शरीर टिका हुआ है, वह धर्म है और जिससे शरीर नहीं टिकता, वह अधर्म है। हम गेहूं पचा सकते हैं, अन्न पचा सकते हैं और यदि हमने पत्थर खाना शुरू कर दिया तो सही नहीं होगा। कोई कहे कि पत्थर तो गेहूं से ज्यादा मज़बूत होता है। लेकिन हमारा शरीर केवल गेहूं से टिकता है, पत्थर से नहीं।
मोर पत्थर खाता है, कंकड़ चुगता है, उसका शरीर पत्थर से ही टिक जाता है। उसके पास पत्थर को हज़म करने की ताक़त है। शरीर के लिए भोजन परिस्थिति के अनुसार ही देना चाहिए। जैसे कोई मरीज है, उसे दाल का पानी, फटा हुआ दूध आदि ही देना है। वही उसके लिए उपयोगी होगा। लेकिन यदि कोई पेचिश का मरीज है, उसे हलवा खिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई हट्टा-कट्टा आदमी है, उसे सिर्फ चार गिलास मट्ठा दिया और कहा कि पूरे दिन ऐसे ही रहो। तो भी गड़बड़ हो जाएगी। उसके शरीर को टिकाने के लिए कुछ रोटी आदि का आधार तो चाहिए। भोजन प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ही चलता है। यदि छोटा-सा बच्चा है, उस बच्चे के अभी दांत भी नहीं निकले हैं, उसे मां का दूध नहीं मिला तो उसे गाय का दूध (जो मां के दूध के सबसे निकट है) पिलाना पड़ेगा। उस समय हम कहें कि नहीं, नहीं इसमें क्या है, बाक़ी लोगों की तरह इसे भी जरा अच्छी-अच्छी रोटी चुपड़कर खिला दी जाए। उस बच्चे का क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए और किसी हट्टे-कट्टे नौजवान को कहा जाए कि वह निपिल से थोड़ा सा दूध पी ले। तब तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए शारीरिक अवस्था और आयु के साथ भोजन का चयन करते हैं।
अब यह नहीं कि यूनीफार्म की तरह भोजन के नियम बना दिए जाएं कि हर व्यक्ति को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वही भोजन दिया जाए। तब तो गड़बड़ हो जाती है। जिस तरह खेत में काम करनेवाले का भोजन दफ्तर में काम करनेवाले बाबू को खिला दिया जाए और बाबू का भोजन खेत के किसान को खिला दिया तो मुश्किल हो जाएगी। सभी का भोजन अलग-अलग होता है। जो सैनिक युद्धभूमि में जाकर लड़ाई करता है, उसे घास-पात का भोजन और जो पंडित घर में बैठकर तप, जाप, वेद-पाठ आदि करता है, उसे मांस खिला दिया जाए तो परेशानी हो जाएगी। भोजन भी प्रत्येक व्यक्ति की धारणा के अनुकूल होना चाहिए। शरीर की धारणा के लिए वैसा ही भोजन करना चाहिए।
लेकिन इतना ही नहीं, इसके आगे भी कुछ है। शरीर का जैसे सुख आवश्यक है, शरीर की धारणा जैसे आवश्यक है, वैसे ही मन का भी विचार करना पड़ता है। उसकी भी आवश्यकता है और जब मन का विचार करेंगे तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह शरीर को स्वस्थ रख सके, वैसे ही मन को भी सुखी रखना चाहिए। मन का सुख नहीं और शरीर का सुख मिल गया तब फिर बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। मन के सुख के लिए ही हमारे यहां कहा गया है कि जहां मन का सुख नहीं, वहां पर कुछ नहीं और जिसे मन का सख प्राप्त है, उसे सब कुछ प्राप्त है। मन सुखी होगा तो तन भी सुखी होगा। जैसे किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई हो, उसे अच्छा-अच्छा भोजन दिया जा रहा हो तो भी उसे कुछ भी नहीं भाता, उसका शरीर भी गिरता जाता है।
आप तो जानते हैं कि अपने यहां गधे के लिए संस्कृत में वैशाखनंदन शब्द का प्रयोग होता है। इसके पीछे किंवदंती है। जब वर्षा के दिन आते हैं। चारों ओर खूब घास होती है तो उस घास को देखकर बेचारा गधा सोचता है कि इतनी ज्यादा घास है, इसको मैं कैसे खाऊंगा और इसलिए उस चिंता के कारण दुबला होता चला जाता है। जैसे अपने कार्यकर्ता स्वयंसेवक भी दुबले होते चले जाते हैं कि इतना बड़ा अपना समाज है, कैसे करेंगे इसका संगठन? यही कारण है कि गधा कितना भी खाता जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसके शरीर को नहीं लगता। लेकिन जब वर्षा ख़त्म हो जाती है। गरमी के दिनों में जेठ और वैशाख की गरमी के कारण घास का एक तिनका भी नहीं दिखाई देता, तब गधा सोचता है कि मैंने कितना पराक्रम कर लिया है। सारी घास खा गया। ऐसा सोच-सोचकर फूलकर कुप्पा हो जाता है।
आदमी भी शायद खाने से मोटा नहीं होता। इसका संबंध मन से है। यदि अच्छा हो तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हम कहीं गए और वहां जाकर खिन्न मन से बैठ गए तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो एक सज्जन ने कहा कि सुगंधि फूल में नहीं, नाक में होती है। मैं कहूंगा कि नाक में भी नहीं, वह मन में होती है। मन अगर ठीक न रहा तो फिर सुगंधि नहीं आएगी।
मन को ही नहीं, इसके साथ-साथ बुद्धि को भी ठीक रखना पड़ेगा। यदि मन भी ठीक है और शरीर भी हट्टा-कट्टा है और केवल बुद्धि ही ठीक नहीं है तो व्यक्ति पागल के समान इधर-उधर भागा फिरेगा। इसलिए सुख यदि चाहिए तो बुद्धि को भी ठीक रखना होगा। जिस तरह मृग रेगिस्तान में दूर मरीचिका देखता है। सूर्य की किरणों के कारण वहां जल का आभास होता है तो वह वहां पानी पीने के लिए पहुंच जाता है। यह ठीक है कि गरमी के दिनों में प्यास तो लगेगी ही। लेकिन उसमें बुद्धि नहीं होती कि वह सोचे कि यह रेत है और सूर्य की किरणों के कारण पानी की तरह दिखाई दे रही है। इसी तरह मनुष्य की ग़लत बुद्धि भी उसे सही रास्ते से हटाकर ग़लत रास्ते पर लाकर पटक देती है।
‘त्रयानात् धूर्तानाम्’ वाली कथा हम सबको मालूम है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण एक बकरी का बच्चा लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसे तीन धूर्त मिले। उन्होंने सोचा कि बकरी का बच्चा इससे लेना चाहिए। एक ने ब्राह्मण को कहा कि अरे महाराज! कहां से आ रहे हो? बोले मेले से आ रहे हैं। वे बोले, ‘कुत्ते का बच्चा क्यों उठा लाए?’ पंडित ने कहा कि यह तो बकरी का बच्चा है। तीनों बोले कि साफ़ दिख रहा यह तो कुत्ते का ही बच्चा है। जब उन तीनों ने ही अपनी बात को परस्पर रखा तो पंडितजी को भी लगने लगा कि शायद उसकी ही बुद्धि धोखा खा रही है। इसलिए उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया। कई बार हमारे अपने ही कारण बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए हमारी यह बुद्धि भी ठिकाने पर होनी चाहिए।
मन, बुद्धि, शरीर के साथ-साथ हमारा एक अहं भी है। उसका भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। जब उसकी पुष्टि नहीं होती तब भी तक़लीफ़ हो जाती है। अनेक प्रकार से मनुष्य को जो कठिनाइयां होती हैं, वे सब उसके अपने अहं के कारण होती हैं। जब अहं का वह ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाता, उसको ठीक प्रकार से तुष्ट नहीं कर पाता, तो उससे तक़लीफ़ हो जाती है। अनेक प्रकार से मनुष्य को सब कठिनाइयां अहं के कारण ही होती हैं। एक बार एक स्त्री नई अंगूठी लाई। किसी का ध्यान उसकी अंगूठी की तरफ़ नहीं गया। वह सोच-सोचकर परेशान थी कि किसी ने पूछा तक नहीं कि वह अंगूठी कहां से लाई। उसने अपने घर में आग लगा ली। जब सभी लोग उस आग को बुझाने आए तो वह अपने अंगूठी वाले हाथ से बताने लगी कि इधर पानी डालो, उधर पानी डालो। एकदम किसी का ध्यान गया तो उसने पूछा कि यह हीरे की अंगूठी कहां से लाई? तो वह बोली कि यदि तुम पहले ही पूछ लेते तो यह आग क्यों लगती। यह जो चीज़ है अहं, उसके अंदर का यह अहं था, वह तृप्त नहीं होता था, इसलिए बेचारी ने आग लगाई। आदमी इसके लिए भी कई बार बड़े-बड़े पाप कर बैठता है। आजकल मनोवैज्ञानिक तो इसका बहुत विचार करके चलते हैं। यह जो अहं है, इसका भी ठीक प्रकार से मेल होना चाहिए।
इस अहं के आगे भी एक तत्त्व है। वह आत्मतत्त्व है, जिसका कि कल भिड़ेजी ने वर्णन किया था। उसका भी आख़िर कुछ-न-कुछ संबंध है। उसका संबंध हमारे जीवन के साथ क्या है? इसका हम थोड़ा-बहुत और विचार आगे करेंगे। इसके साथ-साथ मनुष्य की जब धारणाएं होंगी तो वास्तव में मनुष्य की धारणा होती है। व्यक्ति की धारणा को केवल एक ही चीज़ में ले लिया। किसी ने कहा कि चलो रोटी मिल जाए तो व्यक्ति की धारणा नहीं होगी। यदि इतने से ही व्यक्ति की धारणा हो जाती तो फिर रोटी को छोड़ने वाले लोग नहीं मिलते। मानसिंह ने आख़िर महाराणा प्रताप के यहां भोजन क्यों नहीं किया? यदि भोजन के कारण ही यह धारणा होती तो लोग कहते कि वाह! वाह! भोजन मिल रहा है। पहले भोजन फिर बाद में देखेंगे। ऐसे ही आजकल ब्राह्मणों को कहा जाता है न कि रूखी-सूखी मिले तो कोसों दूर, पूरी-पत्ता मिल जाए तो कोस बारह और नित पाए मालपुआ तो धाए कोस अठारह।
ऐसा ही अगर होता तो ये बाक़ी के व्रत-उपवास करनेवाले और भोजन छोड़ने वाले लोग नहीं मिलते। परंतु उसका बाक़ी के साथ संबंध आता है। इस कारण ही वास्तव में शरीर का विचार करके भी जौहर करनेवाली महारानियां कैसे आ गईं? हम इतना ही मानकर चलते कि शरीर की धारणा होती है। परंतु भोजन के साथ मन का संबंध जोड़ा, इसलिए कभी-कभी भोजन को छोड़कर हम मन की चिंता करते हैं। कभी मन हमें कुमार्ग पर ले जाता है तो उसके ऊपर हम बुद्धि का अंकुश लगा देते हैं। इसलिए धर्म का सद्िवचार करके आदमी चलता है। जहां पर ये सारे विकार आते हैं। कभी-कभी ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि जिस शरीर की धारणा को हमने सार सर्वस्व माना, उस शरीर को छोड़ने पर भी मनुष्य मानता है। ऐसा जैसे कि जौहर करनेवाली रानियां या रणक्षेत्र में अपने प्राणों की बाज़ियां लगा देनेवाला सैनिक। नहीं तो वह यह सोचेगा कि शरीर की धारणा ही सब कुछ है और इसलिए जैसा कि कई लोगों ने कहा कि ‘शरीरमाद्यम खलु साधनम्’ कि शरीर ही सब कुछ है। इसका अर्थ लोगों ने उलटा कर लिया। वास्तव में तो इसका अर्थ यही है कि ‘आद्यम साधनम् शरीरम्’। सबसे पहला साधन शरीर है। इसलिए शरीर को ही प्रमुख मानकर चलना चहिए। वैसा यदि मानकर चलते हैं तो सैनिक सोचेगा कि शरीर बचाओ। शरीर बचा, सब कुछ बच जाएगा। ऐसा विचार करके वह चले तो जैसे ही युद्ध में लड़ने का मौक़ा आएगा, वह तो भाग जाएगा। पहले ही पलायन-वृत्ति उसके मन में आ गई। यह ठीक नहीं है। कभी-कभी तो ठीक है. भागना भी पड़ता है। भगवान कृष्ण भी रणछोड़दास कहलाए। किंतु हर सैनिक यदि रण छोड़कर भागने लगे तो यह ठीक नहीं होगा। सेना का क्या हाल होगा? ज़रा कल्पना करके हम चल सकते हैं।
इस प्रकार इस शरीर से भी कभी-कभी ऊपर आकर विचार करना पड़ता है। जहां पर कि शरीर की धारणा से भी ऊपर उठकर कोई चीज़ है, जिसके आधार पर विचार करके मनुष्य चलता है।
समाप्त
— पाञ्चजन्य, मई 26, 1961, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : लखनऊ