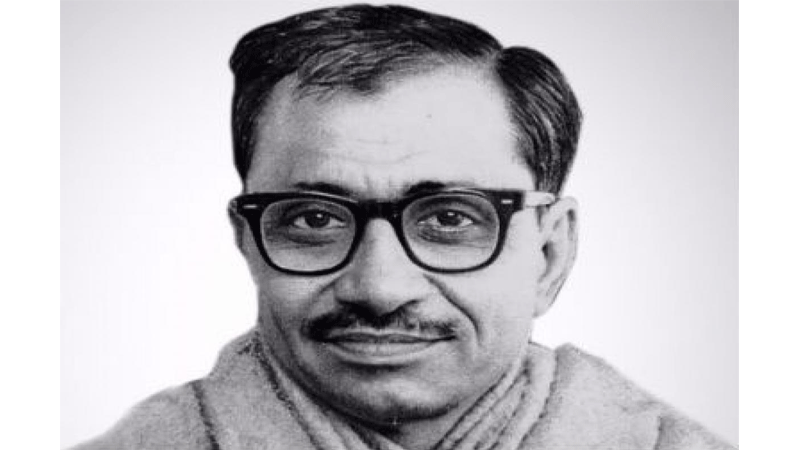दीनदयाल उपाध्याय
जहां तक व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात है, हमें यह मानकर चलना होगा कि व्यक्ति सामाजिक नियमों, समन्वय एवं व्यक्ति और समाज के हितों का समर्थन स्वतंत्र बुद्धि से करेगा। उससे कहा गया कि वह अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग समाज हित में करेगा। यहां तो स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है; जिसका अर्थ होता है कि ‘टारगेट’ पूरे करो। हमारा यहीं पर मतभेद है। जो काम राज्य सौंपे, वही हो, यह क्यों? हम कहना चाहेंगे कि धर्म द्वारा निर्देशित कार्य तथा दैनिक जीवन के व्यवहार ही हमें करणीय हैं।
कुटुंब और पंचायत
व्यक्ति से लेकर राज्य तक की अनेक इकाइयां हमने मानी हैं, परंतु राज्य को ही संपूर्ण समाज का प्रतिनिधि तथा एकमात्र इकाई क्यों माना जाए? कुटुंब भी तो एक इकाई है। समाज कुटुंब के द्वारा अपनी इच्छाओं तथा कामनाओं को व्यक्त करता है, बिना इसके समाज पूरा नहीं होता। कुटुंब के ही ऊपर किसी प्रकार का भार अथवा कर्तव्य पूर्ति का दायित्व डाला जा सकता है। इसलिए हम कुटुंब को एक इकाई मानकर चलें, यही नहीं कुटुंब को हमने राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी एक इकाई माना है। इसी प्रकार हमारे यहां ग्राम पंचायतों को भी एक इकाई माना गया। ये पंचायतें राजाज्ञा पर चलने वाली पंचायतें नहीं हैं। हमारी ये पंचायतें तो स्वयंभू हैं। इसके विपरीत आज ग्राम पंचायतों के लिए ‘ऐक्ट’ बनते हैं, निर्वाचन होता, राज्य के विधायक व मंत्रिगण इनको बनाते हैं, कर्तव्य तथा अधिकार तय करते हैं, इंस्पेक्टर्स नियुक्त होते हैं तथा पंचों के निकालने की व्यवस्था भी बनाई गई है।
जबकि हमारे यहां की ग्राम पंचायतें स्वतंत्र तथा स्वयं-भू इकाइयां रही हैं और जो आदिकाल से चली आती रही हैं। उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। राजा उन्हें आदेश नहीं दे सकता था। राजा के पास एक समिति रहती थी, जिसमें ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि बैठते थे तथा इस तरह ग्राम पंचायतों की बात राजा को सुननी होती थी। यह समिति आज की विधानसभा या राज्य परिषद् की तरह क़ानून बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि केवल शासन चलाने के लिए एक एक्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, ताकि वह सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में काम कर सके। यह प्रतिनिधि राजा के अभिषेक में भाग लेते थे, व्यवस्थाओं में अपनी सम्मति देते थे। स्पष्ट सिद्ध है कि ये लोग राजा की कृपा पर निर्भर नहीं थे, उलटे राजा ही इनके आधार पर खड़ा रहता था।
जात-बाहर करने का भय
ये जनपद और पंचायतें ‘टेरीटोरियल’ आधार पर बनी थीं। ये इकाइयां प्रादेशिक आधार पर ही अधिष्ठित थीं। कार्य की दृष्टि से इकाइयां और श्रेणियां भिन्न प्रकार की थीं। वे अपने कार्य के आधार पर आचरण-धर्म का निर्धारण करते थे, जिसे ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ कहते हैं। इसके विपरीत काम करने वालों का यह श्रेणी बहिष्कार करती थी, स्वयं दंड देती थी। किसी व्यापारी ने मिलावट का व्यवसाय किया तो श्रेणी उसे जाति बहिष्कृत कर देती थी। इस ‘जात-बाहर’ करने की प्रथा का बड़ा भय था। यह लोगों को धर्म पर चलने की प्रेरणा देती थी, यद्यपि आज इसमें अनेक विकार आ गए हैं, संकुचितता आ गई, रूढ़िवादिता आ गई, किंतु इसमें अनेक अच्छाइयां हैं, जिन पर हम सोचते नहीं हैं। यह पद्धति सर्वग्राही पद्धति थी और जिसका दंड भी जीवन के ऊपर समग्र रूप से प्रभाव डालता था। क्योंकि उसमें आज की तरह फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव न थे, प्राचीन वर्णन में लिखा मिलता है- ‘यहां सब जातियों और वर्गों के प्रतिनिधि बैठते थे।” उनकी संख्या भी दी है, प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या वैश्य और शूद्रों की थी, जो क्रमश: 21 और 50 रहते थे; शेष ब्राह्मण या क्षत्रिय चार या छह रहते थे। इस स्वाभाविक अनुपात के अनुसार सभी प्रतिनिधि मिलकर एक मंत्रिमंडल बनाते थे, जिसके सहारे राजा राज्य-कार्य संपन्न करता था। इस मंत्रिमंडल को सारे अधिकार होते थे, राजा बिना समिति और मंत्रिमंडल की सहमति के चाहे जो कर डालने में स्वतंत्र न था।
ऐसे चलते थे राज्य
इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने एक बार यह तय किया कि वह संपूर्ण राज्य की संपत्ति बौद्ध बिहार को भेंट कर देगा। यह प्रस्ताव जब मंत्रिमंडल के समक्ष आया तो उसने ठुकरा दिया। अंत में अशोक ने विवश होकर बौद्ध विहार को एक आंवला भेंट किया और कहा कि “इतना ही केवल मेरा है, शेष सब राज्य की संपत्ति है, मैं कौन हूं जो उसे दे डालूं?” राज्य इसी आधार पर चलते थे। इकाइयों के रूप में हमने उसके क्षेत्र बांटे और उनकी स्वतंत्र व्यवस्था में कभी दखल नहीं दिया।
शिक्षण केंद्रों में कुलपति प्रमुख थे। वही सबके खाने-पीने, पढ़ाई-लिखाई, सब कुछ प्रबंध करते थे। राजा को केवल इस व्यवस्था के लिए धन देना होता था, शेष प्रजा भी उनको धन-संपत्ति दान देती थी। विद्यार्थी ग्रामों में भिक्षा लेने आते थे और सब गृहस्थ भिक्षा देते थे। सभी ध्यान रखते थे कि विद्यार्थी ख़ाली न लौट जाए। कुलपति इसी भांति समाज से, राज्य से सब कुछ संग्रह कर विद्यालय का काम चलाता था। राजा भी यदि पढ़ने जाता तो वही करणीय था उसके लिए। राजा इसमें केवल ‘सुपरविज़न’ करता था, वह भी धर्म के नियंत्रण से उसका काम राजदंड का पालन भर था। शेष क्षेत्रों में उनकी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था थी। जैसा यह था, इसी तरह कुटुंब भी एक स्वतंत्र इकाई थी। उसमें राजा का दख़ल नहीं था। कुटुंब में अव्यवस्था होने पर ही राजदंड का प्रयोग होता था। राजदंड का प्रयोग उस स्थिति में सर्वदा होता भी था।
उन दिनों इस तरह का अपना जो एक समाज था, कह सकते हैं कि उसका कोई केंद्र नहीं था। आजकल इसे विकेंद्रित समाज कहा जाता है, किंतु प्रचलित अर्थों में ऐसी विकेंद्रित अवस्था भी उसमें नहीं थी।
विकेंद्रित का अर्थ है- ‘यदि एक केंद्र की शक्ति समाप्त हो जाए तो भी वहां केंद्रीकरण नहीं रहे।’ वास्तव में इस समाज के अनेक केंद्र रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपने परिवार का सदस्य है, पंचायत का अंग है, व्यवसाय श्रेणी में सदस्य है, राज्य का भी अंग है। सबके साथ जीवन में समन्वय बैठाकर काम चलता जाए, ऐसी एक राज्य व्यवस्था अपने यहां रही है। साथ ही एक बात और है कि जो भी राज्य रहा, उसके लिए धर्म का एक ही आदेश रहा कि समुद्र-पर्यंत यह पृथ्वी एक राष्ट्र है, एक राज्य है। अश्वमेध, राजसूय आदि जितने भी अनेक यज्ञ बनाए गए, उनसे राजा के राजदंड के प्रभाव की प्रस्थापना होती थी। राजा जो यज्ञ करता था, वह संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का यत्न करता था। राम, कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों ने संपूर्ण भारत में एकछत्र राज्य प्रस्थापित किया। भारत की एकता का यह सिद्धांत हम लोगों ने स्वीकार किया। यहां का राज्य अविभाज्य रहा, ऐसा कि जिसका कभी विभाजन या बंटवारा न हो सके। संपूर्ण भारत में एक ही राज्य है, एक ही राज्य रहना चाहिए, एक ही सत्ता रहनी चाहिए, जो कि अनेक सत्ताओं द्वारा बनी हो।
संपूर्ण समाज का काम चलता जाए, इसलिए ‘टेरीटोरियल व सेक्शनल’ आधारों पर अनेक केंद्रों को जोड़कर राज्य बने, परंतु राज्य की अधिसत्ता एक ही व्यक्ति की रहनी चाहिए। राजनीति का यह आदर्श हमारे पूर्वपुरुषों ने रखा है। भारतीय परंपरा है कि राज्य धर्माधिष्ठित हो, धर्मनिष्ठ हो। अतएव आज भी यदि हम आदर्श जीवन व्यवस्था को लाना चाहते हैं तो धर्म का आधार लेकर ही आएगी। यदि इसके विपरीत हुआ तो वह व्यवस्था लादना होगा, वह ग्राह्य न होगी और न टिकेगी ही। आज के युग में ये बातें कुछ अटपटी सी लग सकती हैं। जहां धर्म को मनुष्य का शत्रु मान लिया गया तो वहां समूचे शासन तंत्र को धर्म पर अधिष्ठित करने की बात जल्दी समझ में नहीं आ सकती। पर हम स्मरण रखें कि जब तक इस समस्या पर इतना मूलगामी विचार नहीं होता, मानव की सर्वांगीण उन्नति का मार्ग अवरुद्ध ही बना रहेगा।
-पाञ्चजन्य, नवंबर 20, 1960